भगवद गीता: अध्याय 2, श्लोक 12

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्॥12॥
न-नहीं; तु-लेकिन; एव-निश्चय ही; अहम्-मे; जातु-किसी समय में; न-नहीं; आसम्-था; न-नहीं; त्वम्-तुम; न-नहीं; इमे-ये सब; जन-अधिपा:-राजागण; न कभी नहीं; च-भी; एव-वास्तव में; न-नहीं; भविष्यामः-रहेंगे; सर्वे वयम्-हम सब; अतः-इसके; परम्-आगे।
Hindi translation: ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे।
आत्मज्ञान: जीवन का सार
प्रस्तावना
आत्मज्ञान की खोज मानव जाति के लिए सदियों से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। यह न केवल दार्शनिक चिंतन का विषय है, बल्कि व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग है। इस लेख में हम आत्मज्ञान के महत्व, इसके विभिन्न पहलुओं और इसे प्राप्त करने के तरीकों पर प्रकाश डालेंगे।
आत्मज्ञान का महत्व
प्राचीन ग्रीक दर्शन में आत्मज्ञान
डेल्फी स्थित अपोलो मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण ‘ग्नोथी सीटन’ या ‘स्वयं को जानो’ वाक्य आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाता है। एथेंस के महान दार्शनिक सुकरात ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया और अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
एक रोचक किंवदंती के अनुसार, एक बार सुकरात अपने गहन चिंतन में मग्न होकर चल रहे थे और अचानक किसी व्यक्ति से टकरा गए। उस व्यक्ति ने क्रोध में कहा, “तुम देख नहीं सकते कि तुम कहाँ चल रहे हो, तुम कौन हो?” इस पर सुकरात ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, “मेरे प्रिय मित्र, मैं गत चालीस वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। यदि तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है कि ‘मैं कौन हूँ’, तो कृपया मुझे बताएँ।”
यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कौन हैं और अपने अस्तित्व के बारे में कितना जानते हैं।
वैदिक परंपरा में आत्मज्ञान
भारतीय वैदिक परंपरा में आत्मज्ञान को ज्ञान का आधार माना जाता है। जब ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो उसका प्रारंभ प्रायः आत्म-ज्ञान की शिक्षा से होता है। यह दृष्टिकोण भगवद्गीता में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में समझाते हैं।
आत्मा और शरीर का संबंध
श्रीकृष्ण का उपदेश
भगवद्गीता में श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिसे हम ‘स्वयं’ कहते हैं, वह वास्तव में आत्मा है, न कि भौतिक शरीर। वे बताते हैं कि आत्मा भगवान के समान नित्य है, जबकि शरीर नश्वर है।
श्वेताश्वतरोपनिषद् का दृष्टिकोण
श्वेताश्वतरोपनिषद् में सृष्टि की रचना के बारे में एक महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है:
ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता।
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्तात्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ।।
(श्वेताश्वतरोपनिषद्-1.9)
इस श्लोक का अर्थ है कि सृष्टि की रचना तीन मूल तत्वों के मिश्रण से हुई है: परमात्मा, आत्मा और माया। ये तीनों तत्व नित्य हैं, यानी इनका न कभी आदि था और न कभी अंत होगा।
आत्मा की अमरता
यदि हम आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं, तो यह मानना तर्कसंगत होगा कि भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। यह विचार न केवल हिंदू धर्म में, बल्कि विश्व के कई अन्य धर्मों और दर्शनों में भी पाया जाता है।
आत्मा और पुनर्जन्म
| धर्म/दर्शन | आत्मा की अवधारणा | पुनर्जन्म का विश्वास |
|---|---|---|
| हिंदू धर्म | आत्मा अमर है | हाँ |
| बौद्ध धर्म | आत्मा का अस्तित्व नहीं | हाँ (पुनर्भव के रूप में) |
| सिख धर्म | आत्मा अमर है | हाँ |
| ईसाई धर्म | आत्मा अमर है | नहीं (आम तौर पर) |
| इस्लाम | रूह (आत्मा) अमर है | नहीं |
आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपाय
- ध्यान: नियमित ध्यान अभ्यास से मन शांत होता है और आत्म-चिंतन की क्षमता बढ़ती है।
- स्वाध्याय: आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन आत्मज्ञान के मार्ग में सहायक होता है।
- सत्संग: ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ समय बिताना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है।
- आत्म-विश्लेषण: अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का निरंतर विश्लेषण करना चाहिए।
- सेवा: निःस्वार्थ सेवा से अहंकार कम होता है और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है।
निष्कर्ष
आत्मज्ञान की खोज एक जीवनपर्यंत चलने वाली यात्रा है। यह केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जैसे-जैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं, वैसे-वैसे हमारे जीवन में शांति, संतुष्टि और आनंद का अनुभव बढ़ता जाता है।
आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। यह ज्ञान हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने की शक्ति देता है।
अंत में, यह कहा जा सकता है कि आत्मज्ञान न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज और विश्व के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम दूसरों में भी उसी दिव्यता को देखने लगते हैं, जो सार्वभौमिक प्रेम और शांति की ओर ले जाता है।
Discover more from Sanatan Roots
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



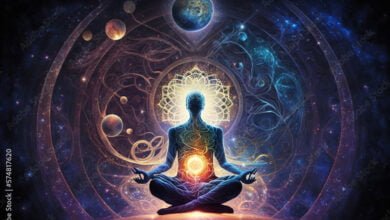
One Comment