भगवद गीता: अध्याय 2, श्लोक 15

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते॥15॥
यम्-जिस; हि-निश्चित रूप से; न कभी नहीं; व्यथयन्ति–दुखी नहीं होते; एते ये सब; पुरुषम्-मनुष्य को; पुरुष-ऋषभ-पुरुषों में श्रेष्ठ, अर्जुन; सम-अपरिवर्तनीय; दुःख-दुख में; सुखम्-तथा सुख में; धीरम्-धीर पुरुष; सः-वह पुरुष; अमृतत्वाय–मुक्ति के लिए; कल्पते-पात्र हे
Hindi translation: हे पुरुषो में श्रेष्ठ अर्जुन! जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव मे मुक्ति का पात्र है।
सुख और दुःख का द्वंद्व: आत्मा की खोज
परिचय
जीवन में सुख और दुःख का द्वंद्व एक सनातन सत्य है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इस द्वंद्व से ऊपर उठने की प्रेरणा दी थी। आइए हम इस गहन विषय को समझने का प्रयास करें और जानें कि आत्मा की सच्ची संतुष्टि कहाँ निहित है।
सुख की खोज: मूल प्रश्न
1. हम सुख क्यों चाहते हैं?
सुख की चाह हमारे अस्तित्व का मूल है। इसके पीछे के कारण हैं:
- आत्मा का स्वभाव: हम परमात्मा के अंश हैं, जो आनंद का अनंत स्रोत हैं।
- स्वाभाविक आकर्षण: जैसे बच्चा माँ की ओर खिंचता है, वैसे ही हम अपने मूल – परमानंद की ओर आकर्षित होते हैं।
- जीवन का लक्ष्य: हर कर्म के पीछे सुख पाने की इच्छा छिपी होती है।
2. भौतिक सुख संतुष्टि क्यों नहीं देता?
भौतिक सुख आत्मा को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे पाता। इसके कारण हैं:
- आत्मा की दिव्यता: आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण दिव्य सुख चाहती है।
- भौतिक सुख की सीमाएँ: संसारिक सुख अल्पकालिक, सीमित और क्षणभंगुर होता है।
- आत्मा की अनंत आकांक्षा: आत्मा अनंत, स्थायी और नित्य सुख की खोज में रहती है।
दिव्य सुख की विशेषताएँ
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| अनंतता | असीमित मात्रा में |
| स्थायित्व | कभी न समाप्त होने वाला |
| नित्यता | सदैव विद्यमान |
भौतिक सुख बनाम दिव्य सुख
भौतिक सुख
- अस्थायी
- सीमित
- जड़वत्
दिव्य सुख (सत्-चित्-आनंद)
- अनंत
- स्थायी
- चेतन
द्वंद्व से ऊपर उठने का मार्ग
- विवेक का विकास: सुख-दुःख के वास्तविक स्वरूप को समझना।
- समभाव का अभ्यास: सांसारिक सुख-दुःख को समान भाव से स्वीकारना।
- आत्मज्ञान की खोज: अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना।
- भक्ति का मार्ग: परमात्मा से जुड़ाव द्वारा शाश्वत आनंद की प्राप्ति।
निष्कर्ष
सुख और दुःख का द्वंद्व जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन इससे ऊपर उठकर आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचानना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। भौतिक सुखों की क्षणिकता को समझकर, हमें अपने अंदर छिपे दिव्य आनंद की खोज करनी चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगा।
आत्मानुभूति की यात्रा
स्वयं को जानने का महत्व
आत्मानुभूति की यात्रा वास्तव में स्वयं को जानने की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। इस यात्रा में:
- हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं
- अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं
- अपने अंतर्निहित दिव्य गुणों को जागृत करते हैं
साधना का महत्व
आत्मानुभूति एक दिन में प्राप्त नहीं होती। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसके लिए:
- नियमित ध्यान: मन की शांति और एकाग्रता के लिए
- स्वाध्याय: आत्मज्ञान के लिए शास्त्रों का अध्ययन
- सत्संग: सद्गुरु और साधकों का सानिध्य
- सेवा: निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा
परमात्मा से एकता का अनुभव
भक्ति का मार्ग
भक्ति मार्ग परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना जाता है। इसमें:
- परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण
- नाम जप और कीर्तन
- प्रेम और श्रद्धा का भाव
ज्ञान का मार्ग
ज्ञान मार्ग आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराता है। इसमें:
- वेदांत का गहन अध्ययन
- आत्म-चिंतन और विचार-मनन
- मिथ्या और सत्य का विवेक
जीवन में संतुलन का महत्व
कर्म और भक्ति का समन्वय
जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति दोनों के लिए कर्म और भक्ति का संतुलन आवश्यक है:
- कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन
- कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना
- फल की चिंता किए बिना कर्म करना
भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन
सच्चा आनंद तभी मिलता है जब हम भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं:
- आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना
- सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाना
- प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना
आत्मानुभूति के लाभ
- मानसिक शांति: चिंता और तनाव से मुक्ति
- आत्मविश्वास: अपनी क्षमताओं पर दृढ़ विश्वास
- करुणा: दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम
- सकारात्मक दृष्टिकोण: जीवन की चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना
- आंतरिक शक्ति: कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की क्षमता
उपसंहार
सुख और दुःख के द्वंद्व से ऊपर उठकर, आत्मानुभूति की यात्रा पर चलना मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह यात्रा हमें न केवल व्यक्तिगत शांति और आनंद प्रदान करती है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देती है। जैसे-जैसे हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, वैसे-वैसे हम दूसरों में भी उसी दिव्यता को देखने लगते हैं। यही वह बोध है जो हमें सच्चे अर्थों में मानव बनाता है और हमारे अस्तित्व को सार्थक करता है।
इस प्रकार, सुख-दुःख के द्वंद्व को समझना और उससे ऊपर उठना न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। हमें अपने दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को उतारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें।
Discover more from Sanatan Roots
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



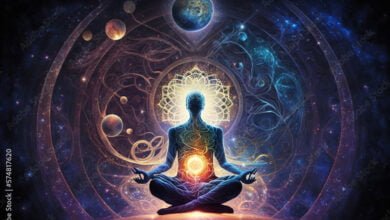
3 Comments