भगवद गीता: अध्याय 1, श्लोक 23

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेयुद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥23॥
योत्स्यमानान्–युद्ध करने के लिए आए योद्धाओं को; अवेक्षे-अहम्–मै देखना चाहता हूँ; ये-जो; एते-वे; अत्र-यहाँ; समागता:-एकत्र; धार्तराष्ट्रस्य-धृतराष्ट्र के पुत्र; दुर्बुद्धेः-हीन मानसिकता वाले; युद्धे युद्ध में; प्रिय-चिकीर्षवः-प्रसन्न करने वाले।
Hindi translation : मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुश्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं।
महाभारत: अर्जुन का अंतर्द्वंद्व और कर्तव्य का मार्ग
प्रस्तावना: कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि
महाभारत का महायुद्ध, भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह केवल दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध की शुरुआत में, अर्जुन ने एक ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव किया, जो उनके जीवन के सबसे बड़े संकटों में से एक था।
धृतराष्ट्र के पुत्रों का कुटिल षड्यंत्र
धृतराष्ट्र के पुत्रों, विशेष रूप से दुर्योधन ने, अपने चाचा पांडु के पुत्रों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखी। उन्होंने पांडवों को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे:
- लाक्षागृह में जलाने का प्रयास
- द्रौपदी का चीरहरण
- जुए में छल करके राज्य हड़पना
- पांडवों को 13 वर्ष का वनवास
इन सभी घटनाओं ने पांडवों के मन में न्याय की मांग को और भी दृढ़ कर दिया।
अर्जुन का प्रारंभिक दृष्टिकोण
युद्ध के पूर्व अर्जुन की मानसिकता
अर्जुन, जो कि महान धनुर्धर और वीर योद्धा थे, युद्ध के प्रारंभ में अत्यंत उत्साहित और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी मानसिकता को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
- न्याय की प्राप्ति: अर्जुन का मानना था कि यह युद्ध उनके और उनके भाइयों के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग था।
- कौरवों के प्रति क्रोध: धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा किए गए अन्याय ने अर्जुन के मन में गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना जगा दी थी।
- कर्तव्य का बोध: एक क्षत्रिय के रूप में, अर्जुन ने युद्ध को अपना धर्म माना और उसे पूरा करने के लिए तत्पर थे।
- विजय का विश्वास: अपने कौशल और श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए, अर्जुन को विजय का पूर्ण विश्वास था।
अर्जुन की प्रारंभिक उक्तियाँ
अर्जुन ने युद्ध के प्रारंभ में जो कहा, वह उनकी तत्कालीन मानसिकता को दर्शाता है:
“हे कृष्ण, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने के लिए व्यग्र हैं। वे अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है।”
यह कथन दर्शाता है कि अर्जुन न केवल युद्ध के लिए तैयार थे, बल्कि वे अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी थे।
युद्धभूमि पर अर्जुन का परिवर्तन
कुरुक्षेत्र में अर्जुन का विषाद
जब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा किया, तब उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके मन को विचलित कर दिया। उन्होंने देखा कि युद्धभूमि में खड़े अधिकांश लोग उनके ही परिवार के सदस्य, गुरुजन, और मित्र थे।
अर्जुन के मन में उठे प्रश्न
- क्या अपने ही परिवार के लोगों को मारना उचित है?
- क्या राज्य प्राप्ति के लिए इतना बड़ा त्याग न्यायोचित है?
- इस युद्ध का परिणाम क्या होगा?
- क्या यह युद्ध वास्तव में धर्म की रक्षा करेगा?
इन प्रश्नों ने अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व उत्पन्न कर दिया।
अर्जुन का विषाद
अर्जुन के मन में उठे विचारों को निम्न तालिका में समझा जा सकता है:
| विचार | भावना | परिणाम |
|---|---|---|
| परिवार का विनाश | दुःख और पीड़ा | युद्ध न करने का विचार |
| गुरुजनों की हत्या | अपराधबोध | धनुष का त्याग |
| राज्य प्राप्ति | लोभ का त्याग | सन्यास लेने का विचार |
| कुल का नाश | भय | युद्ध के परिणामों से डर |
इस मानसिक द्वंद्व ने अर्जुन को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और रथ के पीछे बैठ गए।
श्रीकृष्ण का उपदेश: गीता का ज्ञान
भगवद्गीता का प्रारंभ
अर्जुन की इस स्थिति को देखकर, श्रीकृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि समस्त मानवजाति के लिए एक मार्गदर्शक बन गया।
गीता के मुख्य सिद्धांत
- कर्म का महत्व: श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता किए बिना।
- आत्मा की अमरता: उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए हैं।
- स्वधर्म का पालन: प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।
- निष्काम कर्म: कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाना चाहिए।
अर्जुन के मन का परिवर्तन
श्रीकृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न किया:
- कर्तव्य का बोध: अर्जुन ने समझा कि युद्ध करना उनका क्षत्रिय धर्म है।
- भय का त्याग: मृत्यु के भय से मुक्त होकर, अर्जुन ने युद्ध के लिए मन बनाया।
- निष्काम भाव: राज्य प्राप्ति की इच्छा त्यागकर, केवल कर्तव्य के लिए लड़ने का निश्चय किया।
- धर्म की रक्षा: यह समझ कि युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई है।
युद्ध का प्रारंभ: अर्जुन का नया दृष्टिकोण
कर्तव्यनिष्ठ अर्जुन
गीता के उपदेश के पश्चात, अर्जुन एक नए व्यक्तित्व के साथ युद्धभूमि में खड़े हुए। अब वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कर्मयोगी भी थे।
अर्जुन की नई मानसिकता
- निर्भीकता: मृत्यु के भय से मुक्त होकर, अर्जुन अब बिना किसी संकोच के युद्ध करने को तैयार थे।
- निष्पक्षता: परिवार या मित्र का भेदभाव त्यागकर, वे केवल अपने कर्तव्य पर केंद्रित थे।
- धर्म की रक्षा: युद्ध को अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई के रूप में देखते हुए, अर्जुन ने इसे एक पवित्र कार्य माना।
- निष्काम भाव: राज्य प्राप्ति की इच्छा त्यागकर, अर्जुन केवल अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे थे।
अर्जुन के अंतिम शब्द
युद्ध प्रारंभ करने से पहले, अर्जुन ने कहा:
“हे अच्युत, मेरा मोह दूर हो गया है। मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं संशयरहित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।”
ये शब्द अर्जुन के मन के पूर्ण परिवर्तन को दर्शाते हैं।
निष्कर्ष: अर्जुन का आध्यात्मिक परिवर्तन
महाभारत का युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मानव मन के अंतर्द्वंद्व का भी प्रतीक था। अर्जुन का यह आंतरिक संघर्ष और उसका समाधान हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है।
- कर्तव्य का महत्व: हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।
- निष्काम कर्म: कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाना चाहिए।
- धर्म की रक्षा: हमें हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए।
- आत्मज्ञान का महत्व: सच्चा ज्ञान हमें भय और मोह से मुक्त करता है।
अर्जुन का यह परिवर्तन हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। महाभारत और भगवद्गीता का यह प्रसंग हमें जीवन के गहन सत्यों से परिचित कराता है और हमें अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा देता है।
Discover more from Sanatan Roots
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



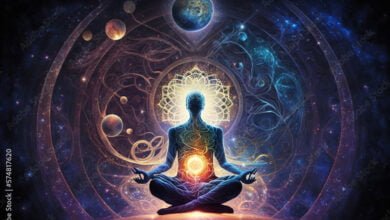
One Comment