भगवद गीता: अध्याय 3, श्लोक 34
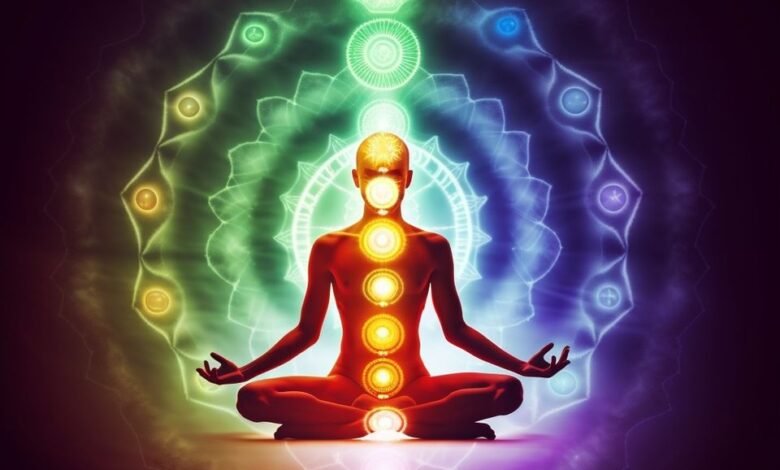
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥34॥
इन्द्रियस्य इन्द्रिय का; इन्द्रियस्य-अर्थ इन्द्रियों के विषयों में; राग-आसक्ति; द्वेषौ-विमुखता; व्यस्थितौ स्थित; तयोः-उनके; न कभी नहीं; वशम् नियंत्रित करना; आगच्छेत्—आना चाहिए; तौ-उन्हें; हि-निश्चय ही; अस्य-उसके लिए; परिपन्थिनौ शत्रु।
Hindi translation: इन्द्रियों का इन्द्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है किन्तु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु हैं।
इन्द्रियों पर नियंत्रण और कर्तव्य-निष्ठा
मन और इन्द्रियों का वश में करना
भगवान श्रीकृष्ण ने पहले ही बल देकर कहा था कि मन और इन्द्रियाँ अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित होती हैं। अब वे इन्हें वश में करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाल रहे हैं। जब तक हमारा भौतिक शरीर हमारे साथ है, तब तक उसकी देखभाल के लिए हमें इन्द्रियों के विषयों का भोग करना पड़ता है। श्रीकृष्ण आवश्यक उपभोग को रोकने के लिए नहीं कहते, बल्कि वे आसक्ति और विरक्ति के उन्मूलन का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं।
पूर्वजन्म के संस्कारों का प्रभाव
पूर्वजन्म के संस्कारों का सभी मनुष्यों के जीवन पर निश्चित रूप से गहन प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि हम गीता द्वारा सिखायी गयी विधि का अभ्यास करते हैं, तब हम अपनी दशा को सुधारने में सफल हो सकते हैं।
इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति
इन्द्रियाँ अपने इन्द्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और उनके आपसी सामन्जस्य से सुख और दुख की अनुभूति होती है। जिह्वा स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने की आदी होती है और कड़वा स्वाद उसे पसंद नहीं आता। मन बार-बार सुख और दुख से जुड़े विषयों का चिन्तन करता है। इन्द्रिय विषयों के सुख के अनुभव से आसक्ति और दुख के अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होती है।
आसक्ति और विरक्ति का उदय
श्रीकृष्ण अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमें न तो अनुकूल परिस्थितियों के लिए ललचाना चाहिए और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करनी चाहिए।
इन्द्रिय विषयों के सुखात्मक अनुभव से आसक्ति और दुखात्मक अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होती है। जब हम किसी विषय में आसक्त हो जाते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं और उसके न मिलने पर दुःख होता है। इसी प्रकार, जब कोई विषय हमें असुखकर लगता है, तो उससे दूर रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।
आसक्ति और विरक्ति का नकारात्मक प्रभाव
आसक्ति और विरक्ति के इन भावों के कारण हमारे मन में सतत् चिंतन और व्याकुलता बनी रहती है। हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं और अपने कर्त्तव्यों का भी ठीक से पालन नहीं कर पाते। इससे हमारे जीवन में अशांति और असंतोष का वातावरण बन जाता है।
श्रीकृष्ण का उपदेश: आसक्ति और विरक्ति से मुक्ति
भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को न तो आसक्ति और न ही विरक्ति के वशीभूत होने को कहा है। वे चाहते हैं कि हम अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समान भाव से रहें। न हम अनुकूल परिस्थितियों में ललचाएं और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराएं।
कर्त्तव्य-निष्ठा और समभाव
जब हम मन और इन्द्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दासता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं और फिर हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन करते समय सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हैं। तब हम वास्तव में अपनी विशिष्ट प्रकृति से मुक्त होकर कार्य करते हैं।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। इन्द्रियों पर नियंत्रण और कर्त्तव्य-निष्ठा से ही हम अपने जीवन को सुखमय और साध्य बना सकते हैं।
जब हम मन और इन्द्रियों के रुचिकर और अरुचिकर दोनों विषयों की दासता से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी अधम प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। हम अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन करते समय सुख और दुख दोनों में समभाव से रहते हैं। यही वास्तविक कर्म-योग है, जिसका अभ्यास करके हम अपने जीवन को साध्य बना सकते हैं।
निष्कर्ष
इन्द्रियों पर नियंत्रण और कर्त्तव्य-निष्ठा से ही हम अपने जीवन को सुखमय और साध्य बना सकते हैं। श्रीकृष्ण का यह महान् उपदेश हमारे लिए एक दिशा-निर्देश है, जिसका हमें सावधानीपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।



4 Comments