भगवद गीता: अध्याय 4, श्लोक 35
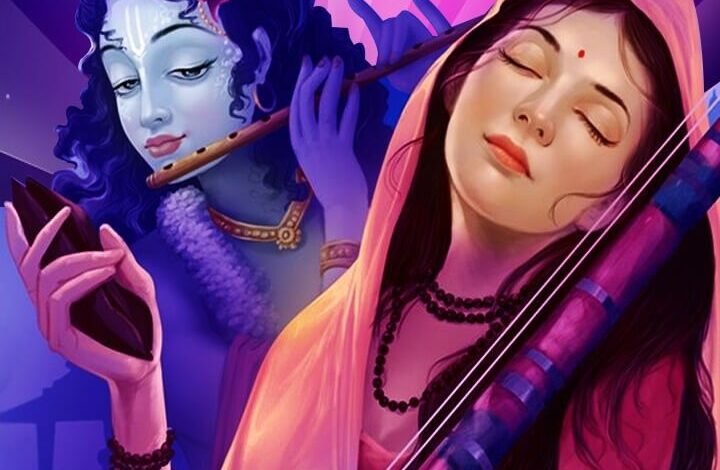
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥35॥
यत्-जिसे; ज्ञात्वा-जानकर; न कभी; पुनः-फिर; मोहम्-मोह को; एवम्-इस प्रकार; यास्यसि-तुम प्राप्त करोगे; पाण्डव-पाण्डव पुत्र, अर्जुन; येन-जिसके द्वारा; भूतानि-जीवों को; अशेषेण-समस्त; द्रक्ष्यसि-तुम देखोगे; आत्मनि-मुझ परमात्मा, श्रीकृष्ण में; अथो यह कहा गया है; मयि–मुझमें।
Hindi translation: इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर, हे अर्जुन! तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझमें स्थित हैं।
भगवत्प्राप्ति: ज्ञानोदय का अद्वितीय मार्ग
प्रस्तावना
जीवन की यात्रा में, हम सभी किसी न किसी प्रकार के ज्ञान की खोज में रहते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है? क्या हमारा वर्तमान ज्ञान हमें सच्ची शांति और आनंद दे पाता है? आइए इस लेख में हम भगवत्प्राप्ति और ज्ञानोदय के महत्व को समझें, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है।
ज्ञानोदय: एक नई दृष्टि
अंधकार से प्रकाश की ओर
जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। यह ज्ञान हमें एक नई दृष्टि देता है, जिससे हम संसार को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं।
मोह का त्याग
ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त करने के बाद, मोह का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जागने के बाद स्वप्न के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है।
भगवत्प्राप्ति का महत्व
निरंतर भगवद्चिंतन
“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः” यह वैदिक मंत्र बताता है कि जो भगवत्प्राप्त हैं, वे सदैव भगवान के परम धाम को देखते रहते हैं। यह स्थिति उन्हें निरंतर आनंद और शांति प्रदान करती है।
दिव्य दृष्टिकोण
भगवत्प्राप्ति के बाद, व्यक्ति संसार को भगवान से अलग नहीं देखता। उसके लिए सब कुछ भगवान की अभिव्यक्ति बन जाता है। यह दृष्टिकोण उसे सांसारिक द्वंद्वों से ऊपर उठा देता है।
माया का प्रभाव
भ्रम का जाल
माया हमें भ्रमित करती है, जिससे हम संसार को भगवान से अलग देखने लगते हैं। यह भ्रम हमें सुख-दुःख के चक्र में फंसा देता है।
मित्रता और शत्रुता का खेल
माया के प्रभाव में, हम लोगों को अपने स्वार्थ के चश्मे से देखते हैं। जो हमारे सुख में सहायक होता है, उसे मित्र और जो बाधक होता है, उसे शत्रु मान लेते हैं।
ज्ञानोदय का प्रभाव
दृष्टिकोण में परिवर्तन
ज्ञानोदय के बाद, व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को भगवान की शक्ति के रूप में देखने लगता है।
सेवा भाव का उदय
ज्ञानी व्यक्ति हर प्राप्त वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है। उसके लिए सब कुछ भगवान का प्रसाद बन जाता है।
सर्वव्यापी भगवत्ता की अनुभूति
सभी में भगवान का दर्शन
ज्ञानोदय प्राप्त संत सभी जीवों में भगवान के अंश को देखते हैं। उनके लिए हर प्राणी भगवान का ही रूप होता है।
हनुमान जी का उदाहरण
रामभक्त हनुमान जी का कथन इस बात को स्पष्ट करता है:
सीय राममय सब जग जानी।
करउँ प्रणाम जोरि युग पानी।।
वे सभी प्राणियों में राम और सीता का रूप देखते हैं और सबको प्रणाम करते हैं।
ज्ञानोदय और भगवत्प्राप्ति का मार्ग
गुरु की भूमिका
ज्ञानोदय के मार्ग पर एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं।
साधना और अभ्यास
निरंतर साधना और आध्यात्मिक अभ्यास ज्ञानोदय के लिए आवश्यक हैं। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है।
शास्त्रों का अध्ययन
वेद, उपनिषद, गीता जैसे शास्त्रों का गहन अध्ययन ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। ये ग्रंथ हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं।
ज्ञानोदय के लक्षण
| लक्षण | विवरण |
|---|---|
| शांति | मन में निरंतर शांति का अनुभव |
| प्रेम | सभी प्राणियों के प्रति निःस्वार्थ प्रेम |
| समता | सुख-दुःख में समान भाव |
| विवेक | सही-गलत का स्पष्ट बोध |
| वैराग्य | भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति |
| सेवा भाव | निरंतर सेवा की प्रवृत्ति |
ज्ञानोदय के बाद का जीवन
निर्लिप्तता
ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। वह कर्म करता है, लेकिन उनके फल से अनासक्त रहता है।
लोक कल्याण
ज्ञानोदय प्राप्त व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता है। वह दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।
आनंद की अनुभूति
निरंतर भगवद्चिंतन में लीन रहने के कारण, ज्ञानी व्यक्ति सदैव आनंद की अवस्था में रहता है। यह आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता।
चुनौतियाँ और समाधान
मन का नियंत्रण
मन को नियंत्रित करना ज्ञानोदय के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन इसमें सहायक हो सकते हैं।
पुराने संस्कारों का त्याग
वर्षों से जमे हुए संस्कारों को बदलना कठिन होता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ इन्हें धीरे-धीरे बदला जा सकता है।
सांसारिक प्रलोभन
भौतिक जगत के प्रलोभन हमें बार-बार आकर्षित करते हैं। विवेक और वैराग्य के अभ्यास से इन पर विजय पाई जा सकती है।
निष्कर्ष
ज्ञानोदय और भगवत्प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। वह सभी में भगवान का दर्शन करता है और निरंतर आनंद की अनुभूति करता है।
इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। दृढ़ संकल्प, नियमित साधना, और गुरु के मार्गदर्शन से हम भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय होता जाता है।
अंत में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ज्ञानोदय केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह हमें समाज और विश्व के प्रति अपने दायित्व को समझने में मदद करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा और मार्गदर्शन के लिए करता है, जिससे पूरा समाज लाभान्वित होता है।
आइए, हम सभी इस दिव्य ज्ञान की खोज में लगें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। याद रखें, यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से साર्थक और फलदायी होगी।



2 Comments