भगवद गीता: अध्याय 1, श्लोक 25

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्।
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥25॥
भीष्म-भीष्म पितामह; द्रोण-द्रोणाचार्य प्रमुखतः-उपस्थिति में; सर्वेषाम्-सब; च और; मही-क्षिताम्-अन्य राजा; उवाच-कहा; पार्थ-पृथा पुत्र, अर्जुनः पश्य देखो; एतान्–इन सबों को; समवेतान्–एकत्रित; कुरून्-कुरु वंशियों को; इति–इस प्रकार।
Hindi translation : भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि हे पार्थ! यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो।
गीता में “कुरु” शब्द का महत्व: एकता और मोह का द्वंद्व
प्रस्तावना
महाभारत के युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करने का आदेश दिया, तब एक ऐसा क्षण आया जो न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व के आध्यात्मिक चिंतन को सदा के लिए बदल देने वाला था। इस महत्वपूर्ण क्षण में, भगवान श्रीकृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया जो सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन जिसमें गहन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक महत्व छिपा हुआ था – वह शब्द था “कुरु”।
“कुरु” शब्द का अर्थ और महत्व
एकता का प्रतीक
“कुरु” शब्द का प्रयोग महाभारत में एक विशेष उद्देश्य के साथ किया गया था। यह शब्द न केवल कौरवों को, बल्कि पांडवों को भी संदर्भित करता था, क्योंकि दोनों ही कुरु वंश के वंशज थे। इस प्रकार, यह शब्द दोनों पक्षों के बीच एक आंतरिक एकता का प्रतीक बन गया।
मोह जागृत करने का माध्यम
श्रीकृष्ण ने इस शब्द का चुनाव बड़ी सावधानी से किया था। उनका उद्देश्य अर्जुन के मन में बंधुत्व की भावना जगाना था, जिससे उसमें मोह उत्पन्न हो सके। यह मोह अर्जुन को विचलित करने के लिए आवश्यक था, ताकि श्रीकृष्ण गीता के महान उपदेश को देने का अवसर प्राप्त कर सकें।
श्रीकृष्ण की रणनीति
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
श्रीकृष्ण की यह रणनीति एक कुशल चिकित्सक की तरह थी। जैसे एक सर्जन पहले रोगी को दर्द निवारक देता है और फिर शल्य क्रिया करता है, वैसे ही श्रीकृष्ण ने पहले अर्जुन के मन में छिपे मोह को जगाया, ताकि बाद में उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके।
दूरदर्शी दृष्टिकोण
श्रीकृष्ण का यह कदम केवल तत्कालीन परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कलियुग के लिए भी था। उन्होंने भविष्य में मानवता के कल्याण के लिए गीता के सिद्धांतों का उपदेश देने की योजना बनाई थी।
“कुरु” बनाम “धृतराष्ट्रतन”
शब्द चयन का महत्व
श्रीकृष्ण ने जानबूझकर “धृतराष्ट्रतन” (धृतराष्ट्र के पुत्र) के बजाय “कुरु” शब्द का प्रयोग किया। यह चयन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि:
- “धृतराष्ट्रतन” शब्द स्पष्ट रूप से केवल कौरवों को संदर्भित करता।
- “कुरु” शब्द दोनों पक्षों को एक साथ जोड़ता है।
परिणाम
इस शब्द चयन के कारण:
- अर्जुन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ।
- युद्ध के औचित्य पर प्रश्न उठे।
- गीता के उपदेश का मार्ग प्रशस्त हुआ।
गीता में “कुरु” शब्द का प्रयोग
प्रथम अध्याय में प्रयोग
गीता के प्रथम अध्याय में “कुरु” शब्द का प्रयोग कई बार होता है। यह प्रयोग अर्जुन के मन में उथल-पुथल मचाने में सफल रहा।
अन्य अध्यायों में संदर्भ
बाद के अध्यायों में भी “कुरु” शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन तब तक अर्जुन का मोह धीरे-धीरे कम होने लगता है।
“कुरु” शब्द का दार्शनिक पहलू
अद्वैत दर्शन का प्रतिबिंब
“कुरु” शब्द का प्रयोग अद्वैत दर्शन के मूल सिद्धांत को दर्शाता है – सभी में एकता। यह दिखाता है कि सतह पर दिखने वाले भेद वास्तव में मिथ्या हैं।
कर्म योग का आधार
यह शब्द कर्म योग के सिद्धांत को भी प्रतिबिंबित करता है। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
“कुरु” शब्द का मनोवैज्ञानिक प्रभाव
अर्जुन पर प्रभाव
अर्जुन पर इस शब्द का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने:
- अपने परिवार के प्रति मोह महसूस किया।
- युद्ध के औचित्य पर सवाल उठाए।
- अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच संघर्ष अनुभव किया।
आधुनिक समय में प्रासंगिकता
आज भी, “कुरु” शब्द का यह प्रयोग हमें सिखाता है कि:
- हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं।
- हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।
- मोह और आसक्ति से मुक्त होना आवश्यक है।
गीता के उपदेश में “कुरु” शब्द का योगदान
मोह से मुक्ति की ओर
श्रीकृष्ण ने “कुरु” शब्द का प्रयोग करके पहले अर्जुन में मोह जगाया और फिर उसे इस मोह से मुक्त होने का मार्ग दिखाया।
कर्तव्य पालन का महत्व
इस शब्द के माध्यम से, गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न हो।
“कुरु” शब्द और आधुनिक जीवन
व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग
हम अपने दैनिक जीवन में “कुरु” शब्द के सिद्धांत को इस प्रकार लागू कर सकते हैं:
- परिवार और समाज में एकता बनाए रखना।
- कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करना।
- मोह और आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास करना।
सामाजिक स्तर पर प्रभाव
समाज के स्तर पर, “कुरु” शब्द के सिद्धांत निम्नलिखित तरीकों से लाभदायक हो सकते हैं:
- सामाजिक एकता को बढ़ावा देना।
- भेदभाव और पूर्वाग्रहों को कम करना।
- सामूहिक कल्याण के लिए काम करना।
निष्कर्ष
“कुरु” शब्द, जो प्रथम दृष्टया एक साधारण शब्द प्रतीत होता है, वास्तव में गीता के संपूर्ण दर्शन का सार है। यह हमें एकता, कर्तव्य और मोह से मुक्ति के महत्व को समझाता है। आज के जटिल और विभाजित समय में, “कुरु” शब्द का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम एक-दूसरे के प्रति सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करें।
“कुरु” शब्द का प्रयोग: एक तुलनात्मक अध्ययन
निम्नलिखित तालिका “कुरु” शब्द के विभिन्न प्रयोगों और उनके प्रभावों को दर्शाती है:
| प्रयोग का संदर्भ | उद्देश्य | प्रभाव |
|---|---|---|
| युद्ध के मैदान में | एकता का बोध कराना | अर्जुन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ |
| गीता के उपदेश में | मोह जगाना और फिर नष्ट करना | अर्जुन को कर्तव्य का बोध हुआ |
| दैनिक जीवन में | सामाजिक एकता बढ़ाना | भेदभाव कम होता है |
| आध्यात्मिक साधना में | अद्वैत भाव जगाना | आत्म-साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है |
इस प्रकार, हम देखते हैं कि “कुरु” शब्द का प्रयोग न केवल गीता में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन और आध्यात्मिक साधना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें एकता, कर्तव्य और आत्म-ज्ञान की ओर ले जाता है।
Discover more from Sanatan Roots
Subscribe to get the latest posts sent to your email.



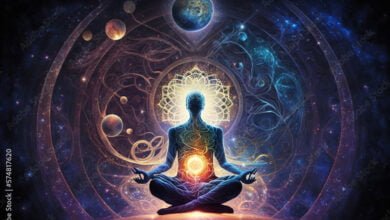
One Comment